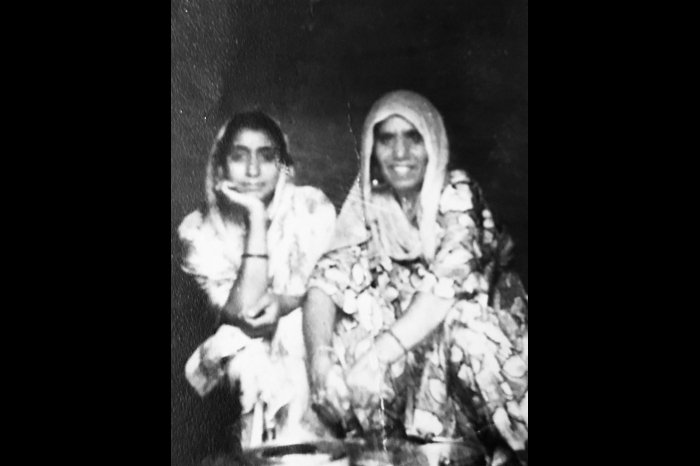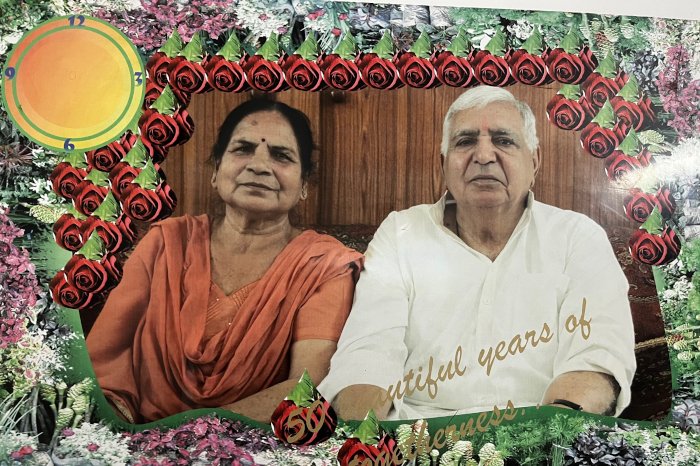पिता जो हमें सर्वशक्तिमान लगते थे (भाग-1)
प्रकाश मनु
भाग—1
पिता के बारे में लिखते हुए उनकी पठानों जैसी क़द-काठी और छवि आँखों में तैर रही है। वे बिल्कुल पठानों जैसे ही थे। सफ़ेद कुरता, सफ़ेद धोती और सिर पर सफ़ेद रंग का ही पग्गड़ . . .! बड़ी-बड़ी और शानदार मूँछें, जिनमें बाद में चलकर तो पूरी सफ़ेदी उतर आई थी। और थोड़ी प्रशांति भी। उनकी यह धज देखते ही बनती। ख़ूब गोरे रंग के, पर चेहरे पर ऐसी लाली कि किसी को भी रश्क हो। कमलेश दीदी कभी-कभी हँसकर कहतीं, “चंदर, हमारे पिता तो बिल्कुल पृथ्वीराज कपूर जैसे हैं!” सुनकर मुझे भी मज़ा आ जाता।
सचमुच बहुत कुछ उनकी धज और चेहरा-मोहरा भी पृथ्वीराज कपूर से मिलता था। कोई एक बार देखे तो भूलना मुश्किल। उनका रोबदाब भी कुछ वैसा ही था।
यों यह धज उनकी तब होती थी, जब उन्हें विशेष रूप से किसी से मिलने या किसी विशेष आयोजन में जाना होता था। नहीं तो पगड़ी सामान्यतः वे नहीं पहनते थे। और कुरता भी ज़्यादा देर तक उनसे नहीं झिलता था। घर से चक्की पर जाते तो कुरता पहनकर और वहाँ जाते ही कुरता उतार देते थे। और फिर उनकी सदाबहार पोशाक बनियान-धोती दिन भर उनका साथ देती। घर लौटते समय फिर वे कुरता पहन लेते।
कुरते के नीचे घर की बनी सफ़ेद मलमल या किसी और मुलायम कपड़े की बनी बनियान ही वे अक्सर पहनते थे, जिसकी बाँहें छोटी होती थीं और उसमें एक जेब बाहर, दूसरी अंदर की ओर गई गहरी जेब होती थी। उसमें वे पैसे वग़ैरह रखते थे। बाहर की जेब में यों ही लिखत-पढ़त की छोटी-मोटी कुछ चीज़ें, या कोई काग़ज़ वग़ैरह। बनी-बनाई जो बनियान बाज़ार से मिलती है, वह उन्होंने कभी नहीं पहनी। ख़ुद पतले, मुलायम कपड़े की बनियान बनवाते थे, जिसकी बनावट बड़ी सादा-सी थी और जो ख़ुद एक छोटी कुरती सी लगती थी। सर्दियों में इसकी जगह कुछ मोटे कपड़े की बनियान आ जाती। यही घर की बनी बनियान और कोई ढाई गज वाली लुंगी की तरह लपेटी जाने वाली सफ़ेद उजली धोती या पंछा, यही सामान्यतः उनकी पोशाक थी, जिसमें वे अक्सर नज़र आते। पर इस सादा सी पोशाक में भी वे ख़ासे जँचते थे और उनके चेहरे की ललछोंही आभा उनके व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण बना देती थी।
अब लिखने बैठा हूँ तो बहुत सी बातें पिता और उनकी आदतों को लेकर तत्काल याद आ रही हैं। यादों की झड़ी सी लग गई है। पर साथ ही लगता है, कि शायद पिता के बारे में लिखना आसान नहीं है। माँ के बारे में लिखना जितना सीधा-सरल है, पिता के बारे में लिखना उतना ही जटिल और मुश्किल काम है। इसलिए कि माँ की तुलना में पिता का व्यक्तित्व भी जटिल था। माँ को जिस तरह से ‘ममता और वात्सल्य की मूरत’ कहता हूँ, पिता को उस तरह से स्नेह और प्यार की मूरत तो नहीं कह सकता। ऐसा नहीं कि पिता ने हमें प्यार न किया हो। पर हिंदुस्तानी घरों में धन कमाना शायद अब भी पुरुष का—स्त्री का नहीं, पुरुष का—पहला पुरुषार्थ है। वह कई बार उसे संतान का मन समझने में असमर्थ बना देता है और माँ के निकट आकर बेटे या बेटी का मन पूरी तरह खुलता है। वही समझ पाती है कि उसकी संतान के भीतर क्या कुछ चल रहा है और उसकी ख़ुशी या फिर उसे सही राह पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है।
पिता यहाँ अक्सर असहाय ही साबित होते हैं जो अक्सर बाहर ही बाहर रह जाते हैं और संतान की भीतरी दुनिया की हलचल से वाक़िफ़ नहीं हो पाते। उन्हें अक्सर बच्चों को जन्म देने वाली अपनी जीवन-सहचरी के ज़रिए ही बच्चों के मन और उनकी ज़िंदों को समझना होता है।
मुझे लगता है कि जैसे पहले क़बीलाई संस्कृति में वीर और बहादुर व्यक्ति ज़मीनें जीतने में लगे रहते थे। यानी आक्रमण करो और जीतो, यही उनका पहला पुरुषार्थ था। बाद की अर्थ-संस्कृति में वही जीतना धन कमाना हो गया। इसीलिए आधुनिकता के आने के साथ-साथ बहुत कुछ बदला, पर पिता की क़बीलाई चरित्र, रूखा और सख़्त चेहरा नहीं बदला। वह अब धीरे-धीरे बदल रहा है, हालाँकि बदलते-बदलते भी अभी शायद उसे सदियाँ लगेंगी!
अलबत्ता माँ से हम जितने खुले हुए थे या जैसी निकटता महसूस करते थे, वैसी न जाने क्यों पिता के साथ नहीं थी। बचपन से ही हम उनसे बात करते डरते थे या कहिए कि बीच में हमेशा एक दीवार जैसी महसूस करते थे। और हमें सुभीता इसी में नज़र आता था कि पिता से जो कहना है, वह माँ की मारफ़त कहा जाए। मानो माँ जो कुछ हम सोचते या चाहते हैं, उसे इशारे भर से जान जाती थीं और यह भी जानती थीं कि पिता से उसे कैसे पास कराना है। माँ जितनी सरल स्नेहमयी थीं, पिता उतने ही जल्दबाद और ग़ुस्सैल। पिता ने, याद पड़ता है कि हमें कभी नहीं पीटा, पर फिर भी जाने क्यों हम पिता के ग़ुस्से से बहुत ज़्यादा डरते थे। उसकी एक आधी वास्तव, आधी कल्पित तस्वीर हमारे ज़ेहन में रहती थी और वह कभी धुँधलाती न थी। यहाँ तक कि कई बार जब हम माँ के क़ाबू में न आते थे, तो माँ को भी हमें डराने के लिए उसका इस्तेमाल करना होता था। और वे कुछ ग़ुस्से में, कुछ हँसते हुए कहती थीं, “आण दे तेरे भाइए नूँ, मैं दस्साँगी।” (आने दो तुम्हारे पिता को, मैं उन्हें बताऊँगी)
“भाइए नूँ . . .!” यानी भाइयाजी को। पिता जी को हम सब भाई-बहन ‘भाइयाजी’ ही कहते थे। पिता जी नहीं, भाइयाजी, जो कभी-कभी जल्दी में ‘भाईजी’ भी बन जाता था। पर मूलतः था वह भाइयाजी ही . . .। ‘भाइयाजी’ पंजाबी शब्द है। इसका हिंदी समानार्थक शब्द ढूँढ़ूँ तो वह होगा भाई, या फिर भाई सरीखा। मैंने कुछ और लोगों के परिवार में भी देखा है। पुराने समय में वहाँ पिता को पिता नहीं, “भाईजी’ या फिर ‘चाचा’ कहा जाता था। पिता को सीधे-सीधे पिता कहना जैसे अच्छा न माना जाता हो। रामविलास जी की ‘घर की बात’ में ऐसे कई प्रसंग हैं। उनके भाई मुंशी जी के बेटे-बेटियाँ उन्हें चाचा ही कहते हैं।
एक कारण यह भी हो सकता है कि संयुक्त परिवारों में पिता अपने बच्चों को अतिरिक्त लाड़ करे, यह अच्छी बात न थी। दूसरे सब तो प्यार करें, पर पिता कुछ दूर ही रहे। तो पिता को घर में बाक़ी सब बच्चे जैसे संबोधित करते थे, उनकी अपनी संतानें भी वैसे ही संबोधित करने लगती थीं। इसीलिए अपने बच्चों के भी वे पिता न रहकर, भाईजी या चाचा हो जाते थे।
मुझे लगता है, संयुक्त परिवारों वाला यह ‘भाइयाजी’ पारंपरिक रूप से तब भी चलता रहा, जब शुरू-शुरू में संयुक्त परिवारों में अलगाव हुआ। बाद की पीढ़ी में यह संबोधन भाइयाजी संभवतः पिता में बदला होगा। पर पिता होते ही, आधुनिकता की मार से वह बड़ी जल्दी डैडी या पापा हो गया . . .। पर हमारे भाइयाजी तो भाइयाजी ही थे। इसके अलावा कोई और संबोधन उनके लिए सटीक ही नहीं लगता।
[2]
पिता ऐसा नहीं कि प्यार न करते हों। बचपन की स्मृतियों को खँगालता हूँ तो पिता को हमेशा थैले भर-भरकर घर में कुछ न कुछ लाते देख़ता हूँ। कभी ढेर सारी जलेबी और इमरतियाँ, कभी संतरे, खरबूजे, अंगूर, केले, अमरूद और भी ढेर-ढेर-सी चीज़ें। लेकिन पिता ने कभी हमें अपनी छाती से नहीं चिपकाया, कभी भाव-विभोर होकर मीठे बोल नहीं बोले। यह सब देखकर माँ कभी-कभी चिढ़कर कहा करती थीं, “तुम्हें तो बस पैसा कमाना आता है। बाक़ी तुमने कुछ सीखा भी है?”
हालाँकि पिता का प्रेम-प्रदर्शन का एक तरीक़ा भी था। हमारी कोई अच्छी बात जानकर या हमारी किसी सफलता के बारे में सुनकर उनकी आँखों में एक तरह की चमक उभरती थी, मूँछें फड़कने लगती थीं और आवाज़ भी कभी-कभी गद्गद् हो जाती थी या फिर काफ़ी मुलायम। सिर गर्व से कुछ तन जाता था, और हम उसी से जान जाते थे कि पिता को यह अच्छा लगा है। बहुत छुटपन का एक प्रसंग याद आता है। पिता को एक बार बहुत लाड़ आया, तो ढेरों छेद वाले निक्के पैसों की माला बनाकर उन्होंने मेरे गले में पहना दी थी। फिर इसी रूप में मुझे घर भिजवाया। किसी नौकर को शायद साथ भेजा था। मैं इसी अनोखी धज में घर पहुँचा तो माँ देखकर पहले तो हैरान हुईं, फिर लाड़ से भरकर बलैयाँ लेती हुई बोलीं, “वेखो नी वेखो, ए आया मेरा राजा पुत्तर . . .!” (देखो री देखो, यह आया मेरा राजा बेटा! )
ऐसे ही माँ ने बताया कि मैं बचपन में मिट्टी बहुत खाता था। इसीलिए मेरे पेट में कीड़े, जिन्हें पंजाबी में ‘मलप्प’ कहते हैं—बहुत हो गए थे। हमारे घर का ज़्यादातर हिस्सा तब कच्चा था। कमरों में फ़र्श न थे। माँ ने कहा, “जैसे भी हो, फ़र्श तो बनवाना ही पड़ेगा। नहीं तो लड़का बीमार पड़ जाएगा।”
यह कठिन दौर था। देश-विभाजन के बाद विस्थापित होकर पिता कुछ अरसा पहले ही आए थे, और जीवन-यापन के लिए कठोर संघर्ष कर रहे थे। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तब घर में चार पैसे आते थे। पर मैं मिट्टी न खाऊँ, इसलिए आर्थिक मुश्किलों के उस दौर में भी पिता ने मेरे छुटपन में, बाक़ी सारे झंझटों और व्यस्तताओं को परे रख, सबसे पहले घर के कमरों में फ़र्श बनवाए। यह भी पिता द्वारा अपनी संतान के लिए प्रेम-प्रदर्शन ही था, लेकिन मूक प्रेम-प्रदर्शन।
पिता जी एक तरह के कर्मयोगी थे। मानो काम करना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूजा हो। बग़ैर काम किए कैसे रहा जा सकता है, उन्हें समझ में नहीं आता था। उनका प्रतिदिन का नियम यह था कि सुबह-सुबह उठकर थोड़ा घूमने जाते और दातुन करते। नीम का दातुन उन्हें बहुत प्रिय था। बचपन में उनके कहने पर हम लोगों ने भी बहुत किया। बड़े हुए तो घर में टूथपेस्ट आ गया। पर पिता को कहीं से अच्छे, ताज़ा दातुन मिल जाते तो ज़ोर देकर कहते, “रोज़ पेस्ट करते हो, आज दातुन करो। इससे पूरा मुँह साफ़ होता है और पेट भी हलका हो जाता है।” और हमें उनकी बात माननी पड़ती।
रोज़ दातुन करने में कोई आधा घंटा तो वे ज़रूर लगाते होंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि सौ बरस की उम्र में जब वे गए, उनके ज़्यादातर दाँत सही-सलामत थे। दातुन के बाद फिर नहाते-धोते और नाश्ता करके चक्की पर चल देते थे। कोई सात बजे चक्की खुल जाती। यों तो उसमें तेल का एक बड़ा एक्सपेलर भी था और रूई की मशीन भी। पर कहलाती वह चक्की ही थी।
चक्की पर पहुँचकर ताला खोलते ही वे सुबह-सुबह लोटा भरकर पानी छिड़कते। फिर झाड़ू-बुहारी करके सामने थल्ले यानी चबूतरे पर गोबर लीपना। फिर धूपबत्ती जलाकर संक्षिप्त पूजा, और उस धूप को भीतर-बाहर ले जाकर वातावरण को पवित्र करना। उसके बाद ही वे कोई और काम करते।
पिता जी को अपने हाथ से काम करने की आदत थी। बल्कि एक ख़ास तरह का आनंद आता था। ख़ुद कुछ निर्मित करने का आनंद। एक बार, मुझे याद है, मुझे साथ लेकर उन्होंने घर के सामने वाले चौक में मेरे लिए छोटी सी चारपाई, जिसे पंजाबी में ‘पघूड़ा’ कहते हैं और हिंदी में पालना, वह बुनी थी। कभी धूप तेज हो जाती तो वे चौक के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जाते, जहाँ छाया होती। पर चारपाई का बुनना निरंतर जारी था। यों थी तो वह चारपाई ही, कोई पालना नहीं, पर बच्चे की चारपाई को ‘पघूड़ा’ ही कहा जाता था। एक सिरे पर पिता जी, दूसरे पर मैं। कोई तीन-चार घंटे तो लगे होंगे, पर ऐसी प्यारी चारपाई बनी कि मुझे अब भी याद है। बुनने के बाद पिता जी ने दौन डालकर उसकी दौन कसी और मुझे भी इसका सही तरीक़ा समझाया। उसके बाद मैं ख़ुद घर की चारपाइयों की दौन कसने लगा।
एक बात और उन्होंने सिखाई, कि अपने काम में शर्म कैसी? आदमी को स्वाभिमानी होना चाहिए। लेकिन उसे मेहनत में शर्म नहीं करनी चाहिए। ख़ूब मेहनत करो, पर किसी से माँगो नहीं, किसी के आगे सिर न झुकाओ। यही उनकी नज़रों में स्वाभिमान था। मेहनत करने से स्वाभिमान पर चोट नहीं आती, दूसरों के आगे हाथ पसारने से स्वाभिमान पर चोट पड़ती है और आदमी को ज़िन्दगी भर इस चीज़ से बचना चाहिए।
थोड़ा मैं बड़ा हुआ, छठी क्लास में आया, तो पिता जी ने एक काम और मेरे ज़िम्मे लगा दिया। बुधवार बाज़ार की साप्ताहिक छुट्टी का दिन होता। उस दिन चक्की बंद रहती और वे घर पर ही होते थे। मैं स्कूल से आता तो वे मुझे पास बैठा लेते, नाते-रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखवाते। पहले हफ़्ते भर जो चिट्ठियाँ आती थीं, वे उन्हें फिर से बाँचने के लिए कहते। फिर पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पर हर चिट्ठी का जवाब लिखवाते। पिता जी के सगे भाई-बहन तो थे नहीं। चाचा-ताऊ के बेटे थे। मेरे वे सब चाचा ही लगे। चाचा मुल्कराज और सोनामल। वे पंजाब के यमुनानगर में रहते थे, जो बाद में हरियाणा में आ गया। परस्पर हालचाल जानने या सुख-दुख की ख़बर के लिए उन्हें चिट्ठियाँ लिखी जातीं। इसी तरह देहरादून में मौसी जी थीं। माँ की वही एकमात्र बहन थीं, उनसे कुछ बरस छोटी। तो मौसीजी और मौसा जी को भी ख़त लिखकर राजी-खुशी ली जाती।
उन दिनों टेलीफोन तो थे नहीं। और वे मोबाइल जो आज घर-घर दिखाई पड़ते हैं और हर कान से चिपके नज़र आते हैं, उनकी तो कोई दूर-दूर तक कल्पना नहीं कर सकता था। चिट्ठी ही हाल-चाल जानने का एकमात्र ज़रिया थी और उसमें भी पोस्टकार्ड ही ज़्यादा लिखे जाते। विस्तार से कुछ लिखना होता तो अंतर्देशीय काम आते। अभिवादन के बाद, “यहाँ सब राजी-खुशी हैं और वहाँ भी ईश्वर की कृपा से सब नेक चाहते हैं।” यह पहला वाक्य लिखा जाता था, जिसे मैं बिना बोले झटपट लिख लेता। फिर “आगे ख़बर यह है कि . . .” के साथ आगे चिट्ठी चलती। पिता जी बोल-बोलकर मुझे लिखवाते। फिर आधी चिट्ठी हो जाती तो कहते, “कुक्कू, पहले इतना ही सुना दे।” मैं सुनाता तो उनके चेहरे पर हलका संतोष दिखाई देता। वे कुछ सोचकर आगे की बात लिखवाते। और अंत में “सब छोटों को प्यार और बड़ों को राम-राम!” इसके लिए जगह रखनी पड़ती। इसलिए कि कभी-कभी छोटे-बड़ों में कुछ के नाम भी लिखवाए जाते।
माँ घर के कामों में लगी होतीं, पर एक कान उनका भी इधर ही लगा होता। तो बीच-बीच में वे भी कोई एकाध बात जुड़वा देतीं। पूरी चिट्ठी लिखवाने के बाद पिता जी एक बार फिर सुनते। कहते, “कुक्कू, अब ज़रा पढ़कर सुना दे।” चिट्ठी सुनकर उनके चेहरे पर अपूर्व संतोष छा जाता, जैसे दूर बैठे रिश्तेदारों से उन्होंने बातें कर ली हों। सबके पते उन्हें मौखिक याद थे। कभी-कभी भूलने पर कृष्ण भाई साहब इसमें मदद कर देते। उन्होंने एक कॉपी में रिश्तेदारों के पते लिख रखे थे। वही हमारी संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त सी डायरेक्टरी थी।
पिता जी ने एक काम और मेरे ज़िम्मे लगाया, हर बृहस्पतिवार को उन्हें और माँ को बृहस्पतिवार की कथा सुनाने का। मुझे याद है, शुरू में तो हमारे यहाँ बस ‘ओम जय जगदीश हरे . . . ’ वाली सीधी-सादी आरती ही होती थी। या फिर एकादशी आदि के व्रत, जिनके लिए किसी लिखित कथा की ज़रूरत न थी। फिर न जाने कब बृहस्पतिवार की कथा शुरू हुई और उसे सुनाने का ज़िम्मा मुझ पर आ गया। मोटे अक्षरों में छपी उस कथा में एक के बाद एक कई घटनाएँ हैं। मुख्य कथा है एक व्यापारी की, जिसे बृहस्पतिवार की कथा और उसके प्रसाद की अवहेलना करने पर सर्वनाश झेलना पड़ा। उसके पास अपार सम्पत्ति थी। पर देखते ही देख़ते उसका सब कुछ तबाह हो गया। माल-असबाब से भरे हुए जहाज़ डूब गए, जवान बेटा न रहा, और भी बहुत कुछ। वह कंगाली की हालत में पहुँच गया। फिर इस दुर्दशा में वह सेठ हर बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगा, तो एक के बाद एक चमत्कार हुए और उसके सुख के दिन लौट आए।
इस पूरी कथा को सुनाने में कोई बीस-पच्चीस मिनट लग जाते। कभी-कभी आधा घंटा भी। कथा के बाद भुने हुए चने और मुनक्के का प्रसाद बाँटा जाता, जिसकी व्यवस्था पूरे साल माँ रखतीं। कुछ समय बाद वह छपी हुई कथा की पुस्तक फटकर जीर्ण-शीर्ण हो गई, तो मैंने उसे हाथ से लिख लिया। पर कथा लंबी थी और एक के बाद एक कई घटनाएँ। मैंने हाथ से लिखते हुए थोड़ी संपादकीय चतुराई से काम लिया, जो उस बाल्यकाल में भी थोड़ी-बहुत तो थी ही। मैंने कथा इस रूप में लिखी कि वह पूरी तो लगे, पर हो संक्षिप्त रूपांतरण। यों संपादन के कारण दोहराव कुछ कम हो गया, संवाद भी मैंने संक्षिप्त कर दिए। मैंने सोचा, “इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है? कहानी तो पूरी हो ही गई। इस तरह कथा सुनाने में हर बार मेरे पाँच-सात मिनट भी बच जाएँगे।” माँ तो मेरी कैशौर्य काल की यह चतुराई न पकड़ सकीं, पर पिता जी ने सुना तो अविश्वास से भरकर कहा, “बस, हो गई कथा पूरी . . .?”
“हाँ, पिता जी . . .!” मैंने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा। पर उन्होंने ग़ुस्से में मेरी ओर देखा, जैसे मेरी चालाकी समझ गए हों। लेकिन अब उसी लिखित कथा को सुनना उनकी लाचारी थी। इस तरह हर बार उस कथा को सुनाने में मेरे पाँच-सात मिनट बच जाते। पिता जी मजबूरी में सुनते तो रहे, पर जैसे उन्हें पूरी तसल्ली न हो। बाद में बृहस्पतिवार की कथा की नई पुस्तक मँगवा ली गई, तो मेरी चालाकी धरी की धरी रह गई। सुबह-सुबह हमारा पढ़ने का समय होता। ऐसे में परेशानी तो होती ही थी। पिता जी से तो कुछ कहने की हम बच्चों की हिम्मत न होती थी। पर माँ झट हमारी बात समझ जाती थीं। मैंने उनसे कहा, “माँ, सुबह-सुबह मेरा पढ़ने-लिखने और स्कूल जाने का समय होता है। ऐसे तो मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊँगा?” इस पर माँ ने सामने वाले मंदिर के पुजारी जी से कहा। वे नियम से घर आकर कथा सुनाने लगे तो मुझे इस ज़िम्मेदारी से छुट्टी मिल गई।
इसी तरह छुटपन में एक और काम मेरे ज़िम्मे था। चक्की पर पिता जी और कृष्ण भाईसाहब के लिए घर से चाय-नाश्ता लेकर जाना। वहाँ आने-जाने में पूरा एक घंटा लग जाता था, जो बहुत अखरता था। इसलिए कि शाम का समय हमारा खेलकूद का समय होता था। भाभी चाय बनाकर बार-बार टेरतीं, “कुक्कू, चक्की पर चाय ले जानी है। चाय ठंडी हो रही है। भाइयाजी डाँटेंगे!”
पर मैं खेल के जोश में होता। इसलिए दूर से पुकारकर कहता, “अभी आया, बस अभी . . .!”
यह अभी बहुत लंबा खिंच जाता तो भाभी फिर याद दिलातीं, चाय फिर से गरम करके देतीं। तो भी डोलू में चक्की तक चाय ले जाने में कई बार चाय ठंडी हो जाती तो डाँट पड़ती थी। साथ ही चक्की के सामने वाले हलवाई से चाय गरम करवा के लानी पड़ती थी।
काफ़ी समय तक यह परंपरा चली। इसके पीछे शायद विचार यह रहा करता था कि घर की चीज़ आख़िर घर की चीज़ है। बाहर वैसा खाना, चाय या नाश्ता भला कहाँ मिल सकता है? बाद में हम बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई का दबाव भी आया तो खाना तो घर से ही जाता था, पर चाय-समोसे वग़ैरह बाहर से ले लिए जाते। यों किशोरावस्था में इन बंधनों से थोड़ी मुक्ति मिली। साथ ही खेल-कूद को बीच में छोड़कर चक्की पर भागने की बाध्यता भी न रही।
[3]
उन दिनों बिजली नहीं थी और मैं पढ़ाकू ऐसा कि कमरे में या छत पर, शाम के स्याह हो जाने तक किताब पर नज़रें गड़ाए पढ़ता रहता था। शायद इस कारण मेरी निगाह कमज़ोर हो गई। यों तो छठी क्लास में ही मुझे समस्या आने लगी थी। अध्यापक द्वारा ब्लैकबोर्ड पर लिखे गए शब्द मेरे ठीक-ठीक पढ़ने में नहीं आते थे। तब मजबूरी में मैं पास बैठे किसी सहपाठी की कॉपी देख-देखकर मैं ब्लैकबोर्ड पर लिखी इबारत को कॉपी पर उतारता था। इसमें अक्सर एक गड़बड़ हो जाती, उस सहपाठी की जो भूलें और वर्तनी की ग़लतियाँ होतीं वे मेरी कॉपी में भी आ जातीं। मुझे पता चल जाता, कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मजबूरी थी। अध्यापक से कुछ पूछने का साहस तब न था।
पर आठवीं या नवीं क्लास में ठीक-ठीक समझ में आ गया कि मेरी निगाह कमज़ोर है। मैंने माँ से कहा, माँ ने पिता जी से और बड़े भाइयों से। जगन भाई साहब तब अलीगढ़ से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके आ चुके थे। पता नहीं उन्होंने बताया या किसी और ने, कि अलीगढ़ में आँखों का बड़ा अस्पताल है, वहाँ दिखाना चाहिए। वह अस्पताल था गाँधी आई हास्पीटल, जो अब भी उतना ही प्रसिद्ध है।
मुझे अच्छी तरह याद है, पिता जी के साथ मैं एक रेलगाड़ी में बैठकर अलीगढ़ गया था। उस अस्पताल का कोई डॉक्टर शायद परिचित भी निकल आया था। पिता जी ने अस्पताल का पता और उस डॉक्टर की जानकारी एक परचे पर लिखवा ली, फिर मुझे लेकर आगरा गए। शायद वह रेलगाड़ी में बैठने का मेरा दूसरी मौक़ा था। इससे पहले बड़े भाई साहब के साथ एक बार आगरा गया था, उसकी याद है। अलीगढ़ शिकोहाबाद से आगरा की तुलना में चूँकि ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए इस बार अपेक्षाकृत लंबी यात्रा थी, जिसमें कोई चार-पाँच घंटे लगे थे।
मुझे याद है, पहली बार जब पिता जी के साथ मैं अस्पताल पहुँचा तो डॉक्टर ने दवा डालकर आँखों की जाँच की। फिर आँखों में डालने के लिए लोकुला ड्रॉप्स देकर कहा, “एक सप्ताह बाद आप लोग आएँ। फिर मैं दोबारा चेक करूँगा। तभी पता चलेगा कि चश्मे की ज़रूरत है, या फिर वैसे ही काम चल जाएगा?”
मुझे याद है, जब पिता जी के साथ शाम को मैं ट्रेन से वापस आया तो मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, “हे प्रभु! चश्मा लग जाए, ज़रूर लग जाए . . . कहीं ऐसा न हो कि डॉक्टर कह दे कि बग़ैर चश्मे के ही काम चल जाएगा!”
शायद मुझे लगा हो कि चश्मा लगाने से मैं कुछ ख़ास हो जाऊँगा। चश्मा उन दिनों बड़ी उम्र के लोग ही लगाते थे। किसी बच्चे को मैंने चश्मा लगाए नहीं देखा था। चश्मा लगने से औरों से कुछ अलग और विशिष्ट होने का रोमांच मैं महसूस कर रहा था। लगता था, इससे औरों पर मेरी बुद्धिमत्ता की छाप पड़ेगी, और इसीलिए मन ही मन चाह रहा था कि अच्छा है, चश्मा लग ही जाए!
अगली बार गया तो डॉक्टर ने फिर से चेक करके बताया कि चश्मा ही लगेगा, तो मैं अंदर ही अंदर ख़ुश और रोमांचित हो रहा था। नीचे आए तो चश्मा बनाने वाली बहुत सी दुकानें थीं। हम लोग सोच ही रहे थे कि कहाँ जाएँ, इतने में एक दुकानदार ने आकर लगभग घेर लिया, “आपको चश्मा लेना है न? आइए-आइए, आप मेरे साथ आइए। आपको बड़ा अच्छा और किफ़ायती फ़्रेम दूँगा। शीशे भी बहुत अच्छे!” और शायद मेरे फ़्रेम पसंद करने के बाद कोई डेढ़-दो घंटे में उसने चश्मा तैयार करके दे दिया। उसी शाम को पिता जी के साथ मैं रेलगाड़ी से वापस लौट आया। चश्मा लगाए हुए . . .। मन ही मन कुछ अटपटा लग रहा था कि अब मित्रों को कैसे फ़ेस करूँगा? उनके तरह-तरह के सवालों के क्या जवाब देने होंगे? . . .
पर इस सब से ज़्यादा अंदर ही अंदर एक गुदगुदी सी हो रही थी। मैं अब चश्मे वाला हो गया। कुछ अलग, कुछ ख़ास। कुछ बच्चे ‘चश्मुद्दीन’ या ‘चश्मेबद्दूर’ कहकर चिढ़ाएँगे, यह बात तो जानता था। पर मैंने सोचा, इसकी क्या परवाह? जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर . . .? चश्मे के कारण खेलकूद में रोज़-रोज़ जो मुसीबतें आएँगी, और चश्मे का लैंस या फ़्रेम बार-बार टूटने पर मेरा सब कुछ थम जाएगा, यह बात तो मैं दूर-दूर तक नहीं सोच रहा था। पर बाद में समझ में आया कि चश्मे के साथ आने वाली मुसीबतें भी कम नहीं हैं।
अलबत्ता चश्मा पिता जी के साथ अलीगढ़ जाकर बनवाया था। यह बात फिर-फिर याद आती है। उस यात्रा की और भी बहुत सी बातें याद आ रही हैं। रेलगाड़ी की खिड़की के पास मैं बैठा था और दूर से दौड़ते पेड़ों और हरे-हरे खेतों की वह छुआछाई आज भी याद है। वह यात्रा लंबी थी, ज़रूर चार-पाँच घंटे लगे होंगे अलीगढ़ पहुँचने में। पर यात्रा सुखद और आनंदकारी थी। रेलगाड़ी की यात्रा बार-बार मन को खींचती है, यह शायद मैंने पहली बार जाना था।
फिर कुछ और बातें भी याद हैं। उन दिनों मेरे बड़े भाई साहब जगन भाईसाहब के विवाह की बात चल रही थी। संभवतः कुछ प्रस्ताव रिश्ते के लिए आए भी थे, पर वे जगन भाईसाहब को पसंद न थे। तो वह ऐसा कुछ गहमागहमी का दौर था। अलीगढ़ प्रवास में किसी दूर के रिश्तेदार के घर ही हम लोग रुके थे। उन लोगों ने हमारी काफ़ी ख़ातिर करने के बाद, बातों-बातों में कैसे रिश्ते की बात चलाई थी और पिता जी को इस सम्बन्ध के लिए मनाना चाहा था, इसकी याद है। पर जगन भाईसाहब अपनी पसंद से विवाह करना चाहते थे। इसलिए पिता जी ने हाँ न करके यही कहा, कि मैं घर पर बात करूँगा। और फिर वह प्रसंग यहीं समाप्त हो गया।
[4]
एक और बात, जिसकी ओर बार-बार मेरा ध्यान जाता है, वह यह कि माँ और पिता का सम्बन्ध बड़ा अद्भुत था। वे झगड़े बग़ैर रह नहीं पाते थे और हफ़्ते में एक-दो बार तो ज़रूर किसी छोटी-मोटी बात पर उलझ जाते थे, पर उनमें आपस में इतना गहरा प्रेम था कि क्या कहा जाए। हाँ, फ़र्क़ यह था कि झगड़ा तो शब्दों में व्यक्त होता था और हम लोगों तक भी उसकी ध्वनियाँ आ जाती थीं, पर प्रेम शब्दातीत था। वह पिता की मूँछों से फिसलती गहरी मुस्कान में व्यक्त होता था और माँ के उस राजमहिषी जैसे गर्व में, जिसके पीछे पिता का प्रेम जीत लेने का विश्वास ही था। यों माँ के साथ पिता का झगड़ा भी, प्यार भी अंत तक चला। अक्सर माँ एक सीमा तक चुपचाप सुनती रहतीं। फिर कहतीं, “बस-बस, हुण बहूँ हो गया!” और आश्चर्य, इसके बाद पिता के मुँह से एक शब्द तक नहीं निकलता था।
इस प्रेम में, आज लगता है, दोनों का एक-दूसरे के प्रति आदर भी ज़रूर शामिल रहा होगा। एक बार की बात मुझे याद है, माँ देहरादून गई थीं, छोटी बहन से मिलने। पीछे पिता थे और हम बच्चे। यह कलकत्ते वालों के मकान की बात है, जहाँ हम कुछ दिन किराए पर रहे थे . . .। सर्दियों के दिन। एक सुबह की बात, पिता कंबल ओढ़े हुए चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। तभी अचानक बीड़ी की राख कंबल पर गिरी। चुपचाप किन्हीं ख़्यालों में खोए पिता को शायद कुछ देर बाद पता चला। जैसे ही ध्यान गया, उन्होंने झट उस राख को झाड़ा। पर तब तक तो उस गरम राख का असर हो चुका था। एक जगह जहाँ राख ज़्यादा गिरी, वहाँ बड़ा सा छेद हो गया, आस-पास कुछ छोटे-छोटे छेद भी।
पिता जी को बड़ा दुख हुआ, नया कंबल था। अब वह भद्दा हो गया। बोले, “पुत्तर, तेरी माँ आएगी तो ग़ुस्सा करेगी। तू ऐसा कर, कहीं से सूई और धागा ढूँढ़कर ला।”
पता नहीं मैं या फिर कमलेश दीदी सूई-धागा ढूँढ़कर लाई। पिता ने उसी समय सूई में काले या किसी गहरे रंग का धागा डालकर कंबल को रफ़ू करना शुरू कर दिया। मुझे अब भी याद है कि उन्होंने कितने जतन, कितनी बारीक़ निगहबानी से यह काम किया था। जब तक कंबल के सारे छेद ढक नहीं गए, तब तक वे बारीक़-बारीक़ रफ़ूगीरी करते रहे। काम पूरा होने पर उन्होंने एक निगाह और कंबल पर डाली। देखकर उनके चेहरे पर संतोष उभर आया। सचमुच पिता ने बड़ी सफ़ाई से रफ़ू किया था। पिता द्वारा रफ़ू किया गया कंबल आज भी मेरी आँखों के आगे से नहीं हटता। वैसे वे घर के कामों में हाथ तक न लगाते थे। पर कोई काम करने पर आ जाएँ तो किस सफ़ाई से करते थे, उनका रफ़ू किया गया कंबल इसकी मिसाल था।
यों पिता को शादियों में कभी-कभार भोजन भी तैयार करते देखा है। तब हलवाई की कम ही ज़रूरत पड़ती थी। बिरादरी वाले ही बड़े उत्साह से काम में हाथ बँटाने के लिए आ जाते थे। उन्हीं दिनों देखा कि पिता यों सामान्यत चाहे भोजन न बनाते हों, पर उन्हें पाक-कला या चीज़ों के अनुपात वग़ैरह का अच्छा ज्ञान था। कभी-कभी होली या ऐसे ही किसी पर्व पर उन्हें घर के आँगन में मीट बनाते भी देखा। यों पिता मीट के शौक़ीन न थे। पर बड़े जीजा जी जिनका ट्रकों का काम था, बढ़िया भोजन के साथ-साथ मीट खाने के भी शौक़ीन थे। तो होली के बाद किसी दिन या वैसे ही साल में एक-दो बार उन्होंने बड़े जीजा जी के साथ मीट तैयार किया था। माँ ऐसे क्षणों में बिल्कुल दूर हो जातीं और अपनी रसोई का इस्तेमाल तक न करने देती थीं। तब शायद कोई बड़ी अँगीठी लाकर आँगन में ही पड़े पतीले में मीट पकाया जाता था।
एकाध बार, याद है, उन्होंने आग्रह करके मुझे भी खिलाया, “ले कुक्कू, कलेजी है, खा ले।” अब कलेजी क्या होती है, मैं क्या जानूँ। पर पिता ने कहा तो सहज ही खा लिया। मेरे घर के पास ही मेरा समवयस्क दोस्त अजमल रहता था। एक दिन खेलते हुए वह मेरे पास आया और कुछ चौंककर उसने कहा, “कुक्कू, तू आज मीट खाकर आया है?”
मैंने झेंपकर कहा, “नहीं तो . . .!”
“वाह, कैसे नहीं!” उसने कहा, “तेरे मुँह से गंध आ रही है मीट की . . .!”
सुनकर याद है, मेरा चेहरा विवर्ण हो गया था। जैसे उस छुटपन में ही मेरे अंदर कोई बैठा था, जिसने चेताया कि कुक्कू, चाहे तूने पिता के कहने पर खाया, पर सच बात तो यह है कि मीट खाना अच्छी बात नहीं है। तब से मीट खाने से मैं बचने लगा। यों घर में बनता ही कितना था। साल में मुश्किल से एक-दो बार, कभी वह भी नहीं।
कुछ और बड़ा हुआ, तो मीट से जुड़ा एक और प्रसंग मुझे याद है। कृष्ण भाई साहब कहीं बाहर से आए, तो देखा एक बड़े पतीले में मीट तैयार है। बस, अभी-अभी वह बनकर तैयार हुआ ही था और किसी ने उसे मुँह तक न लगाया था। न पिता जी ने और न जीजा जी ने। कृष्ण भाईसाहब इससे पहले एक-दो बार पिता जी को टोक चुके थे, “यह अच्छी बात नहीं है कि घर में मीट बने। आपको खाना है तो कहीं बाहर होटल में जाकर खा लीजिए, पर घर में बनाना हमें मंज़ूर नहीं है। फिर आप बच्चों को भी खिलाते हैं, यह और भी बुरी बात है।” पर पिता ने उनकी बातों को हाँ-हूँ कहकर टाल दिया। इसका एक बड़ा कारण जीजा जी थे। वे ही उन्हें जब-तब उकसाते थे, “भाइयाजी, आज तो मीट-शीट हो जाए!” और पिता जी चाहे-अनचाहे तैयार हो जाते थे।
अब तक तो कृष्ण भाईसाहब केवल शब्दों में ही अपनी नाराज़गी प्रकट करके रह जाते थे, पर आज उन्होंने सब्र नहीं किया। बोले, “भाइयाजी, कितनी बार कहा कि घर में मीट नहीं बनेगा। आप बनाते हैं, फिर छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं। क्या यह अच्छी बात है?”
पिता चुप। कृष्ण भाईसाहब आदर्शवादी थे। ग़लत बात कभी नहीं कहते थे, पर ग़लत बात पर टोकने का ज़बरदस्त माद्दा भी था उनमें। पिता जी ने शायद धीरे से बस इतना ही कहा कि “किशन, ठीक है, आगे से नहीं बनेगा।”
पर कृष्ण भाईसाहब का ग़ुस्सा अब तक बेक़ाबू हो चुका था। “तो इस बार भी मैं किसी को नहीं खाने दूँगा।” वे ग़ुस्से में तमतमाते हुए बोले। उन्होंने उसी समय एक कपड़े की मदद से मीट से भरा वह गरम पतीला उठाया और बाहर की ओर चल पड़े। तैयार मीट का पूरा का पूरा पतीला उन्होंने बाहर जाकर नाली में डाल दिया। साथ ही पतीला भी वहीं पटका। फिर बोले, “आज के बाद आपने कभी घर में मीट बनाया तो मैं ऐसा ही करूँगा।”
मुझे याद है, पिता के चेहरे पर उस समय अपने ही बेटे के आगे कैसा अपराध-बोध उमग आया था। चेहरा विवर्ण। उस दिन के बाद न घर में कभी मीट बना और न उन्होंने कभी खाया। जवान बेटे ने सही बात पर टोका था, इसलिए उन्होंने पूरी शान्ति से सहन किया। विरोध में एक शब्द तक नहीं।
पिता सख़्त थे, पर विवेकवान भी। कब झुकना है, वे जानते थे। सही बात चाहे किसी ने कही हो, वह सही है, यह एहसास होते ही झुकना उन्हें अच्छा लगता था। माँ पिता की बातों की बहुत क़द्र करती थीं। पर माँ की सही बात के आगे पिता को झुकते भी मैंने देखा है। यों भी उनकी सख़्ती के भीतर एक मृदुलता थी। इसीलिए माँ के जाने के बाद वे इतने बदल गए कि हमें माँ और पिता दोनों ही लगने लगे। “तेरी माँ होती तो ऐसा कहती . . . या करती!” वे बार-बार कहते थे और ख़ुद भी वैसा ही करने की कोशिश करते थे।
[5]
पिता जी की एक ख़ास बात और याद आ रही है, जो किसी हद तक मुझमें भी आई। उनकी आदत थी, जिस बात की धुन लग जाए, उसे पूरा करके मानना। यह बात हमारे चौक में बने मंदिर को लेकर याद आ रही है, जिसे बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही . . .। असल में, हमारे घर के सामने काफ़ी बड़ा सा चौक है। पिता जी ने देखा, चौक के तीन तरफ़ तो मकान बने हैं, पर एक तरफ़ की ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा ख़ाली है। उनके मन में आया, यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं है। महल्ले की स्त्रियों को गली के दूसरे छोर पर बने एक मंदिर में जाना पड़ता है। उस मंदिर की सीढ़ियाँ भी बहुत ऊँची हैं, जिन पर चढ़ना बूढ़े लोगों और स्त्रियों के लिए आसान नहीं है। उन्होंने सोचा, यहाँ चौक में ही एक सुंदर-सा मंदिर बने तो सबको सहूलियत होगी। साथ ही एक बड़ा-सा हाल और एक धर्मशाला भी हो, तो धार्मिक या अन्य आयोजन भी हो सकेंगे।
उन्होंने महल्ले और बिरादरी के लोगों से बात की तो सभी ने इस विचार को पसंद किया। एक समिति बनी। पैसा इकट्ठा हुआ और ज़मीन का वह टुकड़ा ख़रीद लिया गया। पर मंदिर निर्माण के लिए तो बहुत धन की दरकार थी। पिता जी ने क़रीब दो साल तक व्यवसाय से हाथ खींचा और उसे बेटों के भरोसे छोड़ा। ख़ुद धन एकत्र करने के काम में जुट गए। शहर में बहुत सारे परिचित थे, जो पिता जी की बहुत इज़्ज़त करते थे। उन्होंने आज तक किसी से कभी कुछ न माँगा था। आज एक धार्मिक कार्य के लिए माँगा तो किसी ने मना न किया। जैसे-जैसे पैसे आते गए, निर्माण होता रहा। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने कानपुर और दूसरे अन्य शहरों की भी यात्राएँ कीं, जहाँ व्यवसाय में उनके सहयोगी लोग थे। पिता जी ने आग्रह कर-करके उनसे बड़ी राशि इकट्ठी की। हैरानी की बात यह है कि इसमें धर्म और संप्रदाय का कोई फ़र्क़ न रहा। जिससे भी कहा, उसने खुले हाथों से मदद की।
आख़िर एक सुंदर-सा मंदिर बना, उसका बड़ा-सा भव्य हाल और धर्मशाला भी। पिता जी का मन था कि मंदिर के सामने पीपल का पेड़ हो। उन्होंने अपने हाथ से पीपल का पेड़ लगाया और उसके चारों ओर एक गोल घेरा भी बनवा दिया। आज वह पेड़ इतना बड़ा है कि मंदिर की शोभा तो है ही, साथ ही बहुतों को छाया और सुकून देता है। उसका चबूतरा भी काफ़ी बड़ा हो गया है और वहाँ हर वक़्त छाया में बैठे लोग दिखाई पड़ सकते हैं। पिता जी आज नहीं हैं, पर उनका बनवाया हुआ वह सुंदर मंदिर है, जो पूरे महल्ले को प्रेम, शान्ति और भाईचारे की सीख देता है। और मंदिर के सामने जो बड़ा-सा छतनार पीपल का पेड़ है, उसमें न जाने क्यों, आज भी मुझे पिता का अक्स दिखाई पड़ता है।
बात छोटी सी है, पर यह मंदिर बनवाना उनके लिए तपस्या थी। इसीलिए जिन दिनों मंदिर बन रहा था, पिता जी ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हर वक़्त दौड़ते-भागते ही रहे, ताकि इतना धन हो जाए कि निर्माण अधूरा न रहे। मंदिर की एक-एक ईंट उन्होंने अपने सामने लगवाई। निर्माण में कितना सीमेंट, कितना लोहा, कैसा मसाला बने, एक-एक चीज़ की उन्हें पूरी जानकारी थी। और इसीलिए मंदिर की इमारत भी सादगी के बावजूद सुंदर और भव्य है, ठीक वैसा ही, जैसा उन्होंने चाहा था।
पिता जी की यह ख़ासियत थी कि जो काम उन्हें ठीक लगता था, और जिसे पूरा करने की धुन मन में बैठ जाती थी, उसे वे किए बग़ैर न रहते थे। मेरे और उनके जीवन, और शायद जीवन आदर्शों में भी बड़ा फ़र्क़ है। पर यह चीज़ उनकी किसी हद तक मुझमें भी आई कि जिस काम को करो, उसे पूरा किए बिना मत छोड़ो, चाहे रास्ते में जो भी बाधाएँ आएँ। बढ़ते रहो। अगर मंज़िल तक न पहुँच पाओ, तो भी कम से कम उसकी दुर्निवार तड़प तो बनी ही रहे।
[6]
पिता जी से जुड़ी बचपन की कई यादें हैं। याद पड़ता है, उनके लिए हुक्का भरकर लाने का ज़िम्मा मेरा ही था, और मैं यह काम बड़ी लगन से करता था। हुक्के की चिलम ताज़ा करने का ज़िम्मा भी मेरा ही था। मुझे पता था, पहले चिलम के बीच वाले छेद में एक छोटा सा कोयला रखना है। फिर कहाँ से तंबाकू लेना है, कितना लेना है, यह भी मुझे बता दिया गया था। तंबाकू डालकर माँ से अँगीठी के दो-चार अंगार लेता, और चीमटे से उसे सही ढंग से रखकर ले जाता। देखकर पिता जी ख़ुश होते थे। कई बार अपनी बिरादरी के ही उम्रदराज़ चचा साहिबदत्ता मल आते तो उनसे पिता जी की लंबी बातें छिड़ जातीं। देर तक हुक्का चलता और उसे बीच-बीच में ताज़ा करने का ज़िम्मा मेरा। कभी पानी बदला जाता, तो कभी चिलम ताज़ा करनी होती।
पिता जिस इत्मीनान से हुक्के में गुड़-गुड़ करके धुआँ खींचते, वह मुझे बहुत आकर्षित करता था। और यह भी कि उस समय उनके चेहरे पर कैसा प्यारा सुकून-सा छा जाता है। तो भला हुक्के में ऐसा क्या आनंद है, कि उसके साथ घंटों बातें चलती रहती हैं? यह जानने के लिए एक बार मैंने ख़ुद भी आज़माना चाहा। एक बार जब पिता हुक्का पीकर चले गए और चिलम में अभी आग थी, मैंने भी उन्हीं की तरह हुक्का गुड़गुड़ाने की कोशिश की, पर जल्दी ही साँस फूल गई और कुछ ख़ास मज़ा भी न आया।
“ओह, तो यह ऐसी कला है जो बच्चों के बस की नहीं है। इसमें तो बड़े ही इतना लंबा सुर भर सकते हैं . . .!” मैंने सोचा और आगे से कोशिश छोड़ दी।
उन्हीं दिनों की बात है, एक बार मुझसे बड़ी भूल हुई, जिससे पिता जी के प्राण ही संकट में पड़ गए थे। हुआ यह कि पिता जी खाँसी या ऐसे ही किसी रोग के लिए डॉक्टर से दवा लाए। बादामी रंग की शीशी में वह दवा थी, जो बाहर से दिखाई न देती थी। दवा काफ़ी पहले से चल रही थी। इसलिए संभवतः वैसी ही एक शीशी पहले ख़ाली भी हो चुकी थी। पता नहीं किसी पथ्य या फिर अन्य किसी ज़रूरत के लिए पिता जी उसी पुरानी बादामी शीशी को धोकर, उसमें तेज़ाब ले आए थे। दवा की बादामी शीशी शायद अलमारी के एक कोने में पड़ी थी, तेज़ाब वाली दूसरे कोने में। पर मेरे लिए तो वे दोनों एक जैसी थीं। पिता जी ने अंदर से कटोरी में दवा डालने के लिए कहा, तो मैं भूल से तेज़ाब डालकर ले गया। पिता जी ने वह पिया तो उनकी हालत ऐसी ख़राब हुई कि मुँह से झाग ही झाग निकलने लगा। देखकर सबके हाथ-पैर फूल गए। मुझसे क्या भूल हुई, यह भी सबको जल्दी ही पता चल गया . . . जल्दी से पिता जी को ख़ूब सारा पानी पिलाया गया। फ़ौरन डॉक्टर भी आ गया। दवा शुरू हुई। पर पिता जी को कष्ट बहुत था। उनकी जीभ पर बड़े-बड़े फफोले पड़ गए थे। बल्कि पूरी जीभ ही सूज गई थी। अंदर आँतों में तो घाव थे ही।
मैं छोटा बच्चा, मुझे कुछ पता न था कि हो क्या गया। पर मेरा अंतर्मन कहता था, मुझसे ज़रूर कोई बड़ी ग़लती हुई है जिसके कारण पिता जी की यह हालत हुई है! इतना बड़ा कांड हो जाने पर भी मुझे घर में किसी ने नहीं डाँटा, एक शब्द तक नहीं कहा, पर मैं एक कोने में बैठा-बैठा रो रहा था, और नन्हे मुख से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरे पिता जी ठीक हो जाएँ।
ख़ूब सारा पानी पीकर उलटियाँ करने, और फिर समय पर चिकित्सा मिलने से पिता जी कोई पाँच-सात दिन में ठीक हो गए। उनकी जीभ पर पड़े फफोलों को ठीक होने में तो शायद पंद्रह-बीस दिन लगे। हो सकता है, उन्हें यह घटना बाद में याद भी न रही हो। पर मैं आज भी इसे याद करता हूँ, तो मन में एक थरथराहट सी व्याप जाती है। अगर पिता जी को कुछ हो जाता तो . . .? सोचते ही मेरे प्राण हथेली पर आ जाते हैं। पर इतनी बड़ी घटना हो जाने पर भी पिता जी ने, या घर के और किसी भी व्यक्ति ने मुझे डाँटा नहीं था, यह बात मुझे आज भी याद है।
पिता से जुड़ी कुछ मीठी, मधुर यादें भी हैं। इनमें एक है, जगन भाईसाहब या फिर श्याम भैया के विवाह पर डंडे खेलने वाला नाच। उन दिनों घर में कोई दो दर्जन डंडे बनकर आए तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोई सवा फ़ुट लंबे ये सुंदर और बिल्कुल एकसार डंडे किसलिए? ये तो ऐसे ही थे, जैसे गुल्ली-डंडे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। तब पिता जी ने ही बताया कि डंडे विवाह के समय खेलने के लिए हैं। विवाह के समय खेलने के लिए डंडे . . .! क्या मतलब? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया और उत्सुकता अधीरता में बदल गई।
फिर जब घर से बारात बनकर चली तो पता चला कि यहाँ डाँड नृत्य होना है। आठ-दस लोगों के हाथों में दो-दो डंडे पकड़ाए गए। हर व्यक्ति दोनों हाथों में डंडे लेकर नृत्य की भंगिमा में घूम रहा था, कभी बाईं तरफ़ तो कभी दाईं तरफ़ वाले व्यक्ति के डंडे से डंडे टकराता और फिर दूसरी ओर घूम जाता। इसमें बड़ी अच्छी लय बन जाती और बहुत आनंद आ रहा था। ख़ुद पिता जी बड़ी फ़ुर्ती से डाँड नृत्य में हिस्सा ले रहे थे। मेरी उत्सुकता देखी तो उन्होंने मेरे हाथ में भी दो डंडे पकड़ा दिए गए और मैं भी शामिल हो गया। अब मैं भी उस डाँड नृत्य का हिस्सा था। बड़ा मज़ा आ रहा था, पर मैं लड़का था, जोश ज़्यादा था, तो जब डंडे से डंडा टकराना होता, मैं बड़े ज़ोर से हिट करता। दूसरों को हलके से डंडा आगे बढ़ाते देखता था, पर मैं ऐसी ज़ोर की टक्कर देता कि सामने वाले का हाथ झनझना जाता। पिता जी ने देखा तो इशारे से समझाया, कि “पुत्तर, यहाँ ताक़त लगाने की ज़रूरत नहीं है। डंडे तो हलके से ही खड़काए जाते हैं। चेहरे पर ऐसा लास्य हो कि दूर से लगे, तुम वेग से डंडे चला रहे हो, पर पास आने पर खड़काओ धीरे से। यही कला है।”
पिता जी से जीवन में पहली बार सीखा कला का यह पाठ अब भी याद है।
इसी तरह पिता जी को कभी समाज या बिरादरी में गाते देखूँगा, और ख़ुद चकित मुख सुनूँगा भी, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर बिरादरी की एक-दो शादियों में पिता जी के साथ गया तो उन्हें पुराने लोगों की टोली के बीच हीर गाते सुना। ख़ासकर याद है, ब्रजलाल फंडा के परिवार में किसी का विवाह था और मैं उनके साथ गया था। उसी विवाह से लौटते हुए बारातियों में शामिल बुज़ुर्गों ने एकाएक हीर गाना शुरू कर दिया। मंडली में पहले कोई एक मुखिया के से अंदाज़ में लंबा सुर भरकर कुछ पंक्तियाँ गाता, फिर पीछे-पीछे कोई दूसरा गाता। ऐसे बारी-बारी कथा आगे बढ़ती। उसी मंडली में मैंने पिता को भी लंबा सुर भरकर गाते सुना, जिसमें एक ही शब्द हवा में बहुत दूर तक गूँजता रहता है, और फिर आगे की पंक्ति आती है। गाने की बड़ी पुरानी, पक्के राग जैसी शैली।
मैंने पिता को भी पुराने गवैयों की तरह सुर भरते देखा तो आँखें फैल गईं, “अरे, पिता जी तो गाते भी हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं। अक्सर नहीं गाते तो क्या हुआ? मौक़ा पड़ने पर तो गा सकते हैं और बहुत अच्छा गा सकते हैं। यही क्या कम है?” यह मेरे बाल्य काल की बात है, पर इतना याद है कि पिता को गाते हुए सुनना मेरे लिए रोमांचक था। मुझे बड़े आनंद मिश्रित गर्व की अनुभूति हुई थी।
यों तो पिता जी स्वभाव से धार्मिक थे, पर सामाजिकता और राष्ट्रीयता का भाव भी उनमें कम न था। सन् 1962 में जब चीन का हमला हुआ, उस समय पूरा देश जैसे घायल होकर चीत्कार उठा था। उस समय महल्ले के लोगों की एक बड़ी सभा पिता जी और मेरे बड़े भाइयों ने ही बुलाई थी। अधिकतर पंजाबी बिरादरी के लोग ही आसपास रहते हैं, जो अभी कुछ बरस पहले ही तो उजड़कर पाकिस्तान से आए थे। अब यह नया वार ‘हिंदी चीनी भाई-भाई’ कहने वाले पड़ोसी की ओर से हुआ तो सब तिलमिला गए। पीठ में छुरा घोंपने जैसा अहसास! . . . मुझे ख़ूब याद है, हमारे घर के सामने वाले चौक में सभा हुई थी और सैनिकों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करके भेजने की बात आई थी। पिता जी ने सबसे आगे होकर इसके लिए एक बड़ी राशि देने की बात कही। फिर तो देखते-देखते सभी देश के बहादुर सैनिकों की मदद के लिए कुछ न कुछ देने के लिए आगे आ गए। कौन कितना देगा, सबने वहीं घोषणा की। दो-चार दिन में ही एक बड़ी राशि एकत्र हो गई, जो बिरादरी की ओर से संभवतः प्रधानमंत्री सहायता कोश में भेजी गई थी।
उन दिनों पिता जी रोज़ हमसे अख़बार की ख़बरों के बारे में पूछा करते थे। आस-पड़ोस के लोग मिलकर बैठते और एक ही चर्चा होती थी, कि चीन ने विश्वासघात किया है तो सबको मिलकर उससे लड़ना होगा। जनता कम से कम सैनिकों की मदद करके उनका हौसला और मनोबल तो बढ़ा ही सकती है।
[7]
पिता का स्नेह कभी ज़्यादा बहता नहीं था। वह अधिकतर अव्यक्त ही रहता, किसी शांत अंतर्धारा की तरह। शायद वह ऐसा ज़माना रहा हो कि पिता द्वारा अपनी संतान के लिए प्रेम-प्रदर्शन अवांछनीय, बल्कि ख़राब समझा जाता हो! लेकिन जो भी हो, यह सारी कसर माँ से पूरी होती थी। उनका सारा दिन ‘पुत्तर . . . पुत्तर’ कहते बीतता था और हमारी लगभग हर बात पर ख़ुश होकर ‘हाय नीं मैं वारी जावाँ’ कहते हुए वे हमें छाती से लगा लेती थीं।
इसके बजाय पिता को हम किसी न किसी बात पर टोकते ज़्यादा देखते थे। ख़ासकर किसी चीज़ को बेकार होते देखते तो वे बुरी तरह खीजते थे, “तुम्हें क्या पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। कभी ख़ुद कमाकर देखो तो पता चले!” यह पिता का बार-बार दोहराया गया वाक्य था जो कई बार हमें तिलमिला देता था। लगता था, हम जल्दी ही बड़े हो जाएँ और पिता जी को करके दिखा दें कि हम क्या कर सकते हैं। पर यह बात सोचना जितना आसान था, करके दिखाना उतना ही मुश्किल, यह बड़े होने पर ही पता चला। पिता ने बहुत कठिन संघर्ष करके समाज में एक सम्मानपूर्ण जगह बनाई थी। वे चाहते थे कि हम यह बात जानें, महसूस करें, और इससे सीखें भी, ताकि उनका सब किया-धरा बेकार न चला जाए . . .।
यही कारण है कि पिता सैकड़ों रुपए हम पर ख़र्च कर सकते थे, पर अगर कहीं दो पैसे की चीज़ भी बर्बाद हो रही हो तो उनका ग़ुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुँचता था। अगर हम दिन भर पढ़ते रहे हों और दो मिनट के लिए भी लाइट या पंखा बंद किए बग़ैर कहीं इधर-उधर चले गए, तो उनके लिए यह किसी अक्षम्य अपराध से कम न था। दिन भर हम इतनी लगन और मेहनत से पढ़ते रहे, हमारी इस तपस्या के मुक़ाबले दो मिनट बत्ती या पंखे का चलते रहना कहीं अधिक गुरुतर अपराध था! ज़ाहिर है, पिता ने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया था और यह कमाना हमेशा उनकी चेतना में दस्तक देता रहता था। पर हम शायद इतने ठोस यथार्थवादी न थे। पिता और हमारे अंतर्विरोध का मुख्य कारण भी यही था।
अलबत्ता पिता के बारे में बता ही चुका हूँ कि वे बड़े मेहनती और पुरुषार्थी थे। और वे, मुझे पता चला है, बचपन से ही ऐसे थे। कठोर मेहनत की उन्हें आदत थी और काम से वे क़तई घबराते नहीं थे। ख़ूब कड़ी मेहनत करना और इज़्ज़त, स्वाभिमान और ठसके से जीना—यह मानो उनके जीवन का मूल मंत्र था। कई बार मुझे लगता है, सख़्त मेहनत की जो आदत मुझमें आई, वह शायद पिता से आई। ख़ाली कैसे बैठना चाहिए, यह पिता नहीं जानते और यह शायद मैं भी नहीं सीख पाया।
पिता का गाँव कुरड़-कट्ठा (अब पाकिस्तान में) ख़ुशाब तहसील में पड़ता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबर ने यहाँ के पहाड़ी चश्मे का मीठा पानी पिया और उसकी भरपूर तारीफ़ करते हुए इस स्थान का नाम ख़ुशाब रखा। पिता बचपन में मेहनत का पाठ सीख चुके थे और पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़कर खच्चर पर अनाज वग़ैरह ढोकर ले जाते थे, शहर में बेचने के लिए। एकदम सुबह भोर में ही चलना होता था, ताकि शाम ढलने से पहले घर लौट सकें। बड़ी सख़्त ज़िन्दगी थी, पर अपनी मेहतन से उन्होंने इतना अर्जित कर लिया था कि वे उस इलाक़े के बड़े और सम्माननीय व्यापारियों में गिने जाने लगे थे और लोग आदर से उन्हें ‘शाह जी’ कहते थे। कर्मठता पिता के जीवन और स्वभाव का संस्कार था। इसी तरह व्यवसाय-बुद्धि उनके रक्त में थी। उन्हें मिट्टी दे दो, तो वे पल में उसे सोना बना सकते थे। यह गुण उनमें था। बल्कि कहना चाहिए, व्यवसाय की यह ‘कला’ वे जानते थे। इसे उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, स्वयं अर्जित किया। हालाँकि व्यवसाय में ईमानदारी के वे हमेशा क़ायल रहे और इसी से उनकी एक अलग छवि निर्मित हुई।
2 टिप्पणियाँ
-
19 Apr, 2025 07:19 PM
मैंने आपका पूरा लेख पढ़ा। मुझे अपने माता-पिता की यादें आत्मविभोर कर गईं। - संतोष शर्मा (रामविलास शर्मा की पुत्रवधू), नई दिल्ली
-
9 Apr, 2025 09:17 PM
हमेशा की तरह बहुत ही भावपूर्ण आलेख। पाठक बहता ही चला जाता है आलेख के साथ साथ। उनकी कद-काठी और स्वभाव के बारे में पढ़ते हुए उनका स्वरूप ही दिखाई देने लगा। धन्य है आपका लेखन! --सुकीर्ति भटनागर, पटियाला, पंजाब
कृपया टिप्पणी दें
लेखक की अन्य कृतियाँ
- साहित्यिक आलेख
- कहानी
- कविता
-
- अमृता प्रीतम के लिए एक कविता
- एक अजन्मी बेटी का ख़त
- एक कवि की दुनिया
- कुछ करते-करते हो जाता है कुछ-कुछ
- क्योंकि तुम थे
- गिरधर राठी के लिए एक कविता
- चलो ऐसा करते हैं
- तानाशाह और बच्चे
- तुम बेहिसाब कहाँ भागे जा रहे हो प्रकाश मनु
- त्रिलोचन—एक बेढब संवाद
- दुख की गाँठ खुली
- दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ
- दोस्त चित्रकार हरिपाल त्यागी के लिए
- नाट्यकर्मी गुरुशरण सिंह के न रहने पर
- पेड़ हरा हो रहा है
- बच्चों के मयंक जी
- बारिशों की हवा में पेड़
- भीष्म साहनी को याद करते हुए
- मैंने किताबों से एक घर बनाया है
- मोगरे के फूल
- राम-सीता
- विजयकिशोर मानव के नाम एक चिट्ठी
- हमने बाबा को देखा है
- ख़ाली कुर्सी का गीत
- स्मृति लेख
- आत्मकथा
- व्यक्ति चित्र
- विडियो
-
- ऑडियो
-