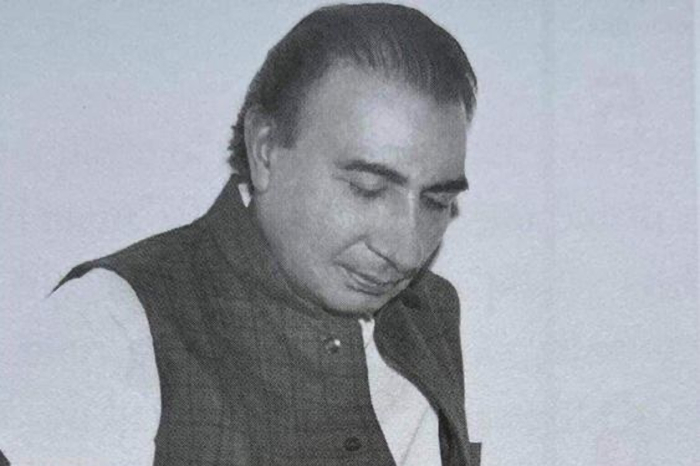गीतसागर के अनमोल मोती!–002–जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ हैं? . . .
सलिल दलाल
गीतसागर के अनमोल मोती!– 002
“जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ हैं? . . .”
कोई कविता एक राष्ट्र को किसी समस्या के बारे में सोचने पर मजबूर करने का काम कितनी सटीकता से कर सकती है, इसका ज्वलंत उदाहरण है ‘प्यासा’ की यह अमर रचना . . . “जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ है?” जैसा कि हिंदी फ़िल्म संगीत के प्रेमी जानते हैं, इस रचना ने साहित्यिक और सामाजिक हलकों में तभी धूम मचा दी थी, जब आज़ादी से तीन-चार साल पहले वह साहिर लुधियानवी के काव्य संग्रह ‘तल्ख़ियाँ’ में प्रकाशित हुई थी। साहिर उस समय कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने अपनी उर्दू कृति ‘चकले’ में उस जगह की क्रूर वास्तविकता का वर्णन किया है, जहाँ महिलाओं के शरीर का व्यापार किया जाता है; जिसे अंग्रेज़ी में ‘रेडलाइट एरिया’ कहा जाता है। उसे गुरुदत्त ने ‘प्यासा’ में अपने अनूठे अंदाज़ में फ़िल्माया और क्लासिक बना दिया।
‘प्यासा’ रिलीज़ होने का साल था 1957। देश नया-नया स्वतंत्र हुआ था। यह उस समय की नेक भावना का कार्य है जब फ़िल्मकार ये सोचते थे कि सिनेमा भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें और फ़िल्में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करें। सोचो कि 1957 के ही वर्ष में ‘प्यासा’ के अलावा ‘मदर इंडिया’, ‘दो आँखें बारह हाथ’ और ‘नया दौर’ जैसी चार फ़िल्में आईं थीं जिनमें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता और उनके व्यापक समाधान को दर्शाया गया था। ‘प्यासा’ में महिलाओं के देह विक्रय की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया, वहीं ‘मदर इंडिया’ में किसानों के शोषण की करुण कथा, ‘नया दौर’ में मशीनीकरण की दौड़ से मेहनतकश लोगों की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी पर असर और ‘दो आँखेंं बारह हाथ’ में जेल सुधारों का क्रांतिकारी सुझाव! याद रहे, इनमें से कोई भी फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री जितनी शुष्क नहीं थी। चारों फ़िल्में टिकट खिड़की पर समान रूप से सुपरहिट थीं।
गुरुदत्त ने जब ‘प्यासा’ में ‘चकले’ को लेने का फ़ैसला किया, तब कहानी के नायक का पेशा बदल गया। मूलतः कहानी गुरुदत्त ने दस साल पहले 1948 में लिखी थी तब उसका नाम ‘कशमकश’ था और नायक एक चित्रकार था। जब गुरु के सहायक राज खोसला ने एक बार उन्हें ‘चकले’ सुनाई, तो गुरुदत्त ने कहा, “बस यही मुझे चाहिए!” राज खोसला ने अपने कॉलेज के दिनों में मंच से यह कविता सुनाकर कई बार वाहवाही लूटी थी। गुरुदत्त ने सोचा कि अगर यह एक नज़्म मिल जाए, तो काम बन जाएगा। लेकिन साहिर लुधियानवी ने एक और रचना ‘ये महलों, ये तख़्तों, ये ताज़ों की दुनिया’ भी दी, जो ‘जिन्हें नाज़ है . . .’ जितनी ही जलाने वाली है। उस के अंतिम शब्द रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ में, “जला दो, जला दो, इसे फूँक डालो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही सँभालो ये दुनिया . . . ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है?” आज भी दुनियादारी से परेशां लोगों के आक्रोश की आवाज़ बनने की क्षमता रखते हैं।
जब ‘प्यासा’ पहली बार वडोदरा में नवरंग टॉकीज़ के मैटिनी शो में देखा था, तब 1967-68 के दिनों में सिनेमा के अँधेरे में मुझे जो रोमांच महसूस हुआ, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। आज यह समझ आ रहा है कि इसके मूल में गुरुदत्त की सशक्त प्रस्तुति थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को ग्लैमराइज़ करने का या तिरस्कार जन्माने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। पूरे गाने के बाद समाज के उस वर्ग के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है। ग़ुस्सा आता है तो सिस्टम पर, सामाजिक व्यवस्था पर! हालाँकि, साहिर के शब्द तो बहुत असरदार थे ही; लेकिन, गुरुदत्त की सादगीभरी कलात्मक दृष्टि, कैमरा एंगल, लाइट शेड की जुगलबंदी और एस.डी. बर्मन की सुलझी हुई संगीत रचना ने समान रूप से योगदान दिया है।
इस रचना की गंभीरता को देखते हुए सचिनदा ने ऑर्केस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं रखा। रिदम भी लगभग ना के बराबर है। यहाँ तक कि गुरुदत्त द्वारा वेश्यालय की महिलाओं के रूप में चुनी गई महिलाओं को देखकर भी लगता है जैसे उन्हें तपेदिक हो गया है! जब भी आप मुंबई के कमाटीपुरा जैसे इलाक़े से गुज़रते हैं या अख़बारों सामयिकों में वहाँ की तस्वीरें देखते हैं, तो गैलरी में खड़ी या खिड़की पर ग्राहकों के इंतज़ार में बैठी महिलाओं के चेहरे पर कोई नूर नहीं दिखता है। साहिर ने गाने में एक जगह लिखा था . . . “ये ढलके बदन और ये बीमार चेहरे . . .” मूल रचना में साहिर साहब ने तो टीबी रोग का नाम तक लिखा था . . . “ये मदकूक चेहरे” यानी ‘तपेदिक चेहरे’!
साहिर ने अपनी मूल उर्दू रचना ‘चकले’ के शब्दों को इस तरह सरल बना दिया कि आम दर्शकों के लिए समझने योग्य हिंदुस्तानी भाषा में रचना को तैयार किया। कविता की ध्रुव पंक्तियाँ कितनी कठिन थीं? “जिन्हें नाज़ हैं हिंद पर वो कहाँ हैं?” के मूल शब्द थे . . . “सना-ख्वाने-तकदीसे-मशरिक कहाँ है?” यानी, “पूर्व की संस्कृति के गुण गाने वाले लोग कहाँ हैं?” जब साहिर ने यह रचना लिखी थी, तब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो यही आवाज़ उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूर्व के सभी देशों में ऐसी महिलाओं के बारे में उठाई थी। साहिर ने इसे, “कहाँ हैं मेरा भारत महान कहने वाले?” जैसे लहजे में बदल कर उसे स्थानीय रंग दे दिया।
गुरुदत्त प्रत्येक अंतरे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मूल रचना के दस अंतरों में से 8 को फ़िल्म में ले लिया!
उन्होंने जो दो अंतरे छोड़े वे भी कहाँ कम थे? मुल्हायजा हों . . .
“ये गूँजे हुए क़हक़हे रास्तों पर
ये चारों तरफ़ भीड़़ सी खिड़कियों पर
ये आवाज़़ें खिंचते हुए आँचलों पर
सना-ख़्वान-ए-तक़्दीस-ए-मशरिक़ कहाँ हैं”
यहाँ साहिर साहब ने शब्दों का जो विरोधाभास रचा है, उसे देखिए। ‘क़हक़हे’ जो घरों में लगते हैं वे रास्ते पर लोग लगाते हैं और भीड़ जो सामान्यतः राहों पर लगती है वो यहाँ, ग्राहक की खोज में खिड़कियों पर लगती है! अगली पंक्ति ये आवाज़़े खिंचते हुए आँचलों पर स्वयं स्पष्ट है। पर अगर ये पंक्ति फ़िल्म में ली गई होती तो गुरुदत्त ने उसे किस अंदाज़ में फ़िल्माया होता ये कल्पना ही कर सकते हैं। उसी तरह से निम्नलिखित पंक्तियाँ भी समाज के लिए उतनी ही शर्मसार करने वालीं थीं, जिसमें महिला की इज़्ज़त के सब से प्राथमिक प्रतीक स्तनों के बदले साहिर ने ‘सीनों’ जैसे शालीन शब्द का प्रयोग किया है। मगर पर्दे पर उन्हें दिखाना, सेन्सर के लिहाज़ से, शायद उन दिनों में सम्भव नहीं होता।
“ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब
ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब
लपकते हुए पाँव ज़ीनों की जानिब
सना-ख़्वान-ए-तक़्दीस-ए-मशरिक़ कहाँ हैं”
आठ अंतरों का गायन होने के बावजूद, उन दिनों में ये बीड़ी-सिगरेट पीने का या वाशरूम ब्रेक लेने की वजह नहीं बनता था। इतने लंबे गाने में फ़िल्मांकन ऐसा है कि आप स्क्रीन से अपनी नज़रें नहीं हटा पाते हैं। साहिर की वर्णनात्मक पंक्ति “तअफ़्फ़ुन से पुर नीम-रौशन ये गलियाँ” का अर्थ है: “ये बदबू से भरी हुई मद्धम रोशनी वाली गलियाँ।” हालाँकि फ़िल्म के लिए इसे सरल कर के “ये सदियों से बेख़ौफ़, सहमी सी गलियाँ” के रूप में बेहतर वर्णित किया गया था। ये ऐसी गलियाँ है, जो दलालों, गुंडों और मवालियों के आधिपत्य के ख़ौफ़ से भरी हुई हैं और उस में रहने वाली महिलाएँ डरी हुई हैं। एक ही पंक्ति में दो विरोधी भावों को सँजोना? भई वाह! गुरुदत्त ने पूरे गाने में ‘मंद रोशनी’ यानी मद्धम प्रकाश ही रखा है। तथाकथित उजले समाज के एक स्याह पक्ष को दिखाने का एक रचनाकार का क्रिएटिव प्रयास!
कविता की शुरूआत ही कितनी चौंकाने वाली है; जो किसी भी संवेदनशील आत्मा को झकझोरने की ताक़त रखती है! सुनिये, “ये कूचे, ये नीलामघर दिलकशी के” मतलब कि आनंद प्रमोद की चीज़ (महिला) की जहाँ नीलामी होती है! भला, औरत के जिस्म की भी नीलामी हो सकती है? फिर “ये लुटते हुए कारवां ज़िन्दगी के” कहने के बाद साहिर पूछते हैं, “कहाँ है कहाँ है मुहाफिज़ ख़ुदी के?” यानी कि “आत्मसम्मान की रक्षा का दावा करने वाले कहाँ हैं?” स्वाभाविक है कि जब एक महिला के शरीर का सौदा किया जा रहा हो तो स्त्री का आत्मसम्मान कहाँ होगा? उनकी चाहत, उनकी संवेदना, उनका प्यार, उनका वात्सल्य किसी की इन बाज़ारों में कोई गिनती नहीं होती है। उन गलियों की इस बात को अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए, गुरुदत्त इस गीत से पहले कोठे पर एक नाट्यात्मक दृश्य खड़ा करते हैं।
हालाँकि ये नज़्म सेक्सवर्करों के दर्द को बयाँ करने के लिए लिखी गई है; पर उन दिनों सिनेमा जैसे माध्यम की जिन मर्यादाओं का फ़िल्मकार स्वयं पालन करते थे, इस के कारण उस जगह को नाचने वाली का कोठा बताया गया था। उस सीन में एक महिला डांस कर रही होती है और बग़ल के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उसका बच्चा भूखा है, उसको स्तनपान कराने की चिंता और उसे गोद में उठाने की उत्सुकता से नाच कर रही महिला विनती भरी नज़रों से अपने ग्राहकों की ओर देखती है। उनमें से एक शराब का ख़ाली गिलास दिखाता है और उसे शराब से भरने का इशारा करता है! बच्चे को स्तनपान कराना या ग्राहक को शराब पिलाना? जब वह अपने बच्चे को प्राथमिकता देकर अगले कमरे में गई तो कोठे की मैडम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस महफ़िल में धकेल दिया।
वह चिल्लाती है, “मेरा बच्चन बीमार है” और एक ग्राहक आदेश देता है, “बच्चे को मार गोली . . . हम भी तो बीमार हैं। पहले हमारा इलाज कर, बाद में बच्चे को संभाल।” ग्राहक नर्तकी के हाथ में पैसे रखता है और फिर से तबले पर थाप! बिना अपने मन के मगर अपनी संतान की चिंता में नाचती ‘बाईजी’ का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया और महफ़िल में बैठे गुरुदत्त की आँख से एक आँसू उनके हाथ में लिए शराब के प्याले में गिर गया। मानो मदिरा की मस्त मिठास में किसी के आँसुओं का खारापन भी हो। गुरुदत्त शराब के उस गिलास के साथ यह गाना गाते (या गुनगुनाते?) हुए उस देह के बाज़ार से गुज़रते हैं। हर शब्द बेमिसाल है मगर हमारा पसंदीदा प्रयोग है ‘बेख़्वाब बाज़ार’। एक ऐसा मार्केट जिस में सपने नहीं देखे जा सकते, क्योंकि वहाँ पूरी रात कोई सोता ही कहाँ है? इस नज़्म पर गुरुदत्त ने क्या शॉट कंपोजीशन किया है! “ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार” जैसे जुमलों को चित्रित करते समय हाई लाइट और लो लाइट का किया हुअ उपयोग। औरत की इज़्ज़त, उसके सतीत्व एवम् शील के सौदे और फिर क़ीमत को लेकर विवाद! मानो वह महिला कोई इंसान नहीं मवेशी हो। जब ‘गुरु’ “ये इस्मत के सौदे” पंक्ति गाते हैं, तो बाईजी उनके पीछे तकरार करती हुई दिखाई देती हैं। जब “सौदों पे तकरार” गाया जाता है तो गुरुदत्त यह कहना चाहते होंगे कि इस व्यापार में भी हो रहे भाव-ताल पर झगड़ों से समाज को शर्मिंदा होना चाहिए।
पूरे गाने में सचिनदेव बर्मन ने केवल दो बिंदुओं पर ताल का प्रयोग किया है। वो उजले दरीचों में पायल की ‘छन छन’ के दौरान घुँघरू की छनछनाहट की आवाज़ आती है और अगली पंक्ति “तबले की धन धन” में तबला के तोड़े की दो या तीन आवाज़ें आती हैं। उस अंतरे की तीसरी पंक्ति में बेबस औरत की खांसने की आवाज़ के साथ साहिर के बेहतरीन शब्द . . . “वो बेरूह कमरों में खाँसी की ठनठन”! खांसने की आवाज़ उस कमरे से आ रही है जहाँ बिना आत्मा वाला सिर्फ़ निष्प्राण ‘शव’ पड़ा है; सेक्स को एन्जोय करने वाली स्त्री नहीं! क्या वेश्यालय का इससे अधिक काव्यात्मक तथा यथार्थवादी वर्णन सम्भव हो सकता है? गुरुदत्त इस रचना की गंभीरता से परिचित थे और इसलिए जैसे-जैसे कविता अपने चरम की ओर बढ़ती है, वे देह व्यापार में पड़ी महिलाओं की पहचान कराते हुए अपने चेहरे पर सम्भव उतना दर्द लाकर ये शब्द गाते हैं, . . .
“ये बीवी भी है और बहन भी है माँ भी . . .” हाथ में शराब का गिलास गालों पर दबाते हुए गुरुदत्त दो बार गाते हैं। महिलाओं के ये रूप समाज को दिखाई क्यों नहीं देते? उन्होंने शीशे को दर्पण का प्रतीक माना होगा। अगली पंक्तियों में वे इस भावना से कि उन महिलाओं की मुक्ति के लिए कुछ किया जाना चाहिए, सुझाव देते हैं मगर साहिर अपनी अनुपम शैली की इन पंक्तियों में . . .
“मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी
यशोदा की हम-जिन्स, राधा की बेटी
पयम्बर की उम्मत, जुलैखा की बेटी
जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ है?”
साहिर ने हमेशा की तरह सभी धर्म याद किये! यह आदम और ईव की बेटी है, जो प्रकृति की ‘पहली महिला’ के ईसाई विचार को बढ़ावा देती है जिस के मुताबिक़ वह विश्व की प्रथम माता है। तो उन्होंने यशोदा की लैंगिक जाति की याद दिलाने के लिए शब्द चुना ‘हम जिन्स’! जिन्स का वैज्ञानिक मतलब आज तो सब जानते हैं; मगर 1957 में अपने गाने में लाना? सिर्फ़ साहिर ही कर सकते थे! उन्होंने कोई स्त्री राधाजी की पुत्री होने का भी हवाला देकर हिंदुओं को झकझोर दिया, वहीं पैग़म्बर और जुलैखा की दुहाई देकर इस्लामी विचारधारा वाले समाज को भी स्त्रियों की उस स्थिति के लिए आग्नेय प्रस्तुति की! फ़िल्म में इन पंक्तियों के आने से पहले गुरुदत्त फिर से एक नाटकीय दृश्य का उपयोग करते हैं। एक महिला को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोठे में ले जाते हुए देखा जा सकता है। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और जो लोग उसे ले जा रहे हैं वे उसे मजबूर करते हैं। गुरुदत्त सह नहीं सकते और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया जाता हैं।
खड़े होकर नायक ये पंक्तियाँ गाता है . . . “मदद चाहती है हव्वा की बेटी।” दरअसल, उस सीन से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि ऐसी उत्पीड़ित महिलाओं के उपरांत, गुरुदत्त यानी ‘विजय’ जैसे संवेदनशील सामान्य लोग, जो उन्हें बचाना चाहते हैं, उन को भी मदद की ज़रूरत है। (‘प्यासा’ में गुरुदत्त का नाम ‘विजय’ था। लेकिन वे अमिताभ बच्चन वाले ‘हीरो’ नहीं थे जो एक साथ दस लोगों को मार सकता था, ये तो एक आदमी के धक्के से भी गिर जानेवाला सामान्य व्यक्ति था!) उस बदनाम बस्ती में आनेवालों को गिनाते समय भी साहिर लिखते हैं यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनौ-मंद बेटे भी अब्बा मियाँ भी . . . यहाँ वे सीनियर के लिए ‘पीर’ शब्द का प्रयोग करते हैं; मगर तंदुरस्त व्यक्ति के लिए ‘सेहत मंद’ नहीं पर तनौ-मंद को उपयोग में लाते हैं। वह ‘70 के दशक में उर्दू समझना सीखनेवाले हम जैसे नौसिखियों के लिए, बिना कम्प्यूटर या ऑनलाइन उपलब्धताओं के दिनों में, हमारे एक दोस्त काज़ी द्वारा एक नया आयाम खुलने जैसा था।
साहिर अंत में लिखते हैं कि ऐसी समस्या के लिए कोई अकेला व्यक्ति उन मज़लूमों की मदद नहीं कर सकता, वे पूरे समाज को पुकारते हैं, मगर अपने ही अंदाज़ में . . .
“ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ
ये कूचे, ये गलियाँ, ये मंज़र दिखाओ
जिन्हें नाज़ है हिन्द पर उन्हें भी बुलाओ
जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ है?”
देश के नेताओं को इस वेश्यालय में लाओ! ये शब्द साहिर ने फ़िल्म के लिए बदला था। मूल शब्द थे . . . “बुलाओ, ख़ुदाए-दीन को बुलाओ!” यानी धर्म के ठेकेदारों को यहाँ बुलाओ। जब यह रचना आज़ादी से पहले लिखी गई थी तब सामाजिक संरचना में धार्मिक व्यवस्थाएँ मूल में थीं। लेकिन देश को आज़ाद हुए दस साल हो गये थे। राजनीतिक नेता (मुल्क के रहबर-नेता) अब राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ज़िम्मेदारी उठा रहे थे, न कि धार्मिक नेता। एक ख़ास बात यह भी नोट करने की आवश्यकता है कि समाज सुधार का ऐसा संदेश देने वाला राजनीतिक ऐंगल गुरुदत्त को कितना भाया होगा पता नहीं। क्योंकि उन्होंने ‘प्यासा’ के अलावा अपनी पिछली फ़िल्मों में या उसके बाद की फ़िल्मों में भी ऐसा कोई सोशल स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन इस के साथ ही यह भी कहना होगा कि इसका पूरा श्रेय गुरुदत्त को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने ‘चकले’ सिर्फ़ सुनकर ही उसको अपने चलचित्र में लेने की हिम्मत दिखाई। गुरु ने साहिर के एक-एक शब्द को आत्मसात किया और किताब की नज़्म को एक सेल्युलोइड कविता बना दिया!
आज जब हम हर जगह फ़िल्म संगीत के नाम पर निरर्थक तुकबंदी सुनते हैं, तब ऐसे कालजयी गीत को याद करते हुए यह कहने का मन होता है, “कहाँ है? कहाँ हैं? साहिर जैसे शायर . . . और गुरुदत्त जैसे डायरेक्टर!”
*********
‘प्यासा’ की कुछ अधिक जानकारियाँ . . .
-
‘प्यासा’ 22 फरवरी 1957 को मुंबई के मिनर्वा थिएटर में रिलीज़ हुई थी। अपने समय से पहले आई इस फ़िल्म को भारत में ‘नेशनल’ से लेकर ‘फ़िल्मफेयर’ तक का कोई भी एवार्ड नहीं मिला था। जैसा कि पिक्चर में होता है, रचनाकार के जाने के बाद उन पर प्रशस्तियों की बौछार हुई है। पूना फ़िल्म इन्स्टिट्युट जैसे सिनेमा के संस्थानों में ‘प्यासा’ को पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाता है।
-
‘प्यासा’ बड़े बड़े आंतरराष्ट्रिय सामयिकों और समीक्षकों ने बरसों बरस उसे विश्व की श्रेष्ठ 100 और 25 फ़िल्मों की सूची में शामिल किया है। पर भारत में ‘दादा साहेब फाळके’ तो छोड़िए, गुरुदत्त को पद्मश्री भी नहीं मिला था! हां, उनकी फिल्मों के नियमित कैमेरामेन वी.के. मूर्ति एक मात्र टेक्निश्यन बने, जिन्हें दादा साहेब फाळके’ से पुरस्कृत किया गया था।
-
गुरुदत्त ने मुख्य भूमिका के लिए दिलीप कुमार को चुना था। लेकिन, शूटिंग के पहले दिन काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी दिलीप साहब नहीं आए तो गुरुदत्त ने ख़ुद मेकअप चढ़ा लिया और ‘कवि’ बन गए विजय!
-
फ़िल्म में काव्यसंग्रह का शीर्षक ‘आप की परछाइयां’ है, जो साहिर की मशहूर प्रलंब कविता ‘परछाइयां’ की याद दिलाता है।
-
‘जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है?’ और ‘ये महलों ये तख़्तों, ये ताज़ों की दुनिया’ जैसे विस्फोटक गीत और उनके बोल तथा संगीत बहुत लोकप्रिय हुए और परिणामस्वरूप गुरुदत्त की अगली फ़िल्म ‘कागज़ के फूल’ को भी एस.डी. ने संगीतबद्ध किया था। परन्तु, बर्मन दादा के मुक़ाबले साहिर ने अपनी ‘फीस’ एक रुपया ज़्यादा माँगी और ‘गुरु’ ने साहिर को छोड़कर कैफ़ी आज़मी को ले लिया। ये प्रसंग फ़िल्मसंगीत में शब्दों और कवि/शायर का महत्त्व दिखाने के लिए साहिर के योगदान के रूप में हमेशा याद रखा गया है। कहा जाता है कि गुरुदत्त उन्हें एस.डी. बर्मन के समान वेतन देने को तैयार थे। फिर भी साहिर ने शब्दों की महत्ता को प्रस्थापित करने के लिए एक रुपया अधिक लेने का अपना तर्क नहीं छोड़ा था। हालाँकि, उस नये चित्र का काव्यात्मक नाम ‘कागज़ के फूल’ साहिर ने ही गुरुदत्त को दिया था।
-
‘प्यासा’ में जॉनी वॉकर पर फ़िल्माया तेल मालिश वाला गाना ‘सर जो तेरा चकराए’ ‘एसडी’ ने नहीं बल्कि उनके टैलेंटेड बेटे राहुल देव बर्मन ने कंपोज किया था।
-
‘जिन्हें नाज़ है . . .’ फ़िल्म में शुरू होने से पहले की स्थिति हैदराबाद में एक कोठे की यात्रा के दौरान गुरुदत्त के अनुभव का फ़िल्मांकन मात्र है। अंतर केवल इतना था कि हैदराबाद की एक नर्तकी गर्भवती थी और ग्राहकों ने उस पर नृत्य करने के लिए ज़ोर डाला, जबकि वह अपनी गर्भावस्था के सातवें महीने में थी।
-
‘प्यासा’ की मूल कहानी बहुत पहले गुरुदत्त ने लिखी थी, तब इसका नाम ‘कश्मकश’ रखा गया था। फ़िल्म में माला सिन्हा द्वारा निभाया गया ‘मीना’ का किरदार मधुबाला को निभाना था। जब दिलीप कुमार उस फ़िल्म में नहीं रहे तब मधुबाला भी निकल गईं। फ़िल्म में मूलतः वहीदा रहमान का किरदार नहीं था। लेकिन ‘देवदास’ की सफलता और इस रचना ‘चकले’ को फ़िल्म में शामिल करने से फ़िल्म की पृष्ठभूमि बदली गई। चित्रकार के स्थान पर नायक ‘शायर’ बन गया। ‘देवदास’ की ‘चंद्रमुखी’ की
तरह यहाँ ‘गुलाब’ को लाया गया। नायक की प्रेमिका की अमीर आदमी से शादी भी ‘देवदास’ की ‘पारो’ की याद दिलाती है। वर्षों बाद, दिलीप कुमार ने ख़ुलासा किया कि लगातार निराशावादी नायकों के चित्रण के कारण वे मानसिक रूप से परेशान थे। इसलिए आख़िरी वक़्त पर ‘प्यासा’ छोड़ दी थी। -
पैसे को लेकर गुरुदत्त से साहिर की नहीं बनी तो दोनों अलग हो गये। हालाँकि, 26 जनवरी 1962 को फ़िल्मफ़ेयर से साक्षात्कार में, साहिर ने कहा कि प्यासा की सफलता के बाद, निर्माताओं ने साहित्यिक गीतों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था।
-
वितरकों की माँग के कारण गुरुदत्त को ‘प्यासा’ का अंत बदलना पड़ा। वैसे तो फ़िल्म मालासिन्हा और गुरुदत्त के बीच आख़िरी मुलाक़ात के साथ समाप्त होती थी। जिसमें क्रेन से टॉपशॉट के साथ शायर की कविताओं के पत्र हवा में उड़ रहे हैं। वितरकों को वह अंत बहुत निराशावादी लगा। अंत में, गुरु ने ‘विजय’ के हाथों में नाचने वाली ‘गुलाबों’ हाथ डालकर डूबते सूरज की किरणों में जाते हुए दिखाकर एक सुखद अंत दिया। ‘प्यासा’ हिट हो गई। जिस तरह से ‘कागज़ के फूल’ निराशावादी अंत के साथ फ़्लॉप हुई, उसे देखते हुए, शायद वितरक सही थे!!
1 टिप्पणियाँ
-
1 Aug, 2023 06:53 PM
बहोत ही सुंदर लेख।इतनी बारीकियों से कभी देखा, सुना ,या सोचा नहीं। फीर से पूरा गाना देखना ही पड़ेगा।